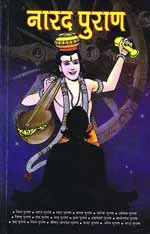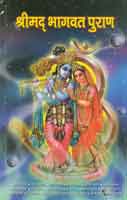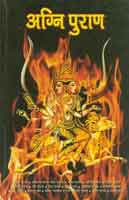|
पुराण एवं उपनिषद् >> नारद पुराण नारद पुराणविनय
|
171 पाठक हैं |
||||||
पुराण-साहित्य-श्रृंखला में नारद पुराण....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय जीवन-धारा में जिन ग्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण
भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराण साहित्य
भारतीय जीवन और साहित्य की अक्षुण्ण निधि हैं। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष
और अपकर्ष की अनेक गाथाएँ मिलती हैं। कर्मकांड से ज्ञान की ओर आते हुए
भारतीय मानस चिंतन के बाद भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। विकास की
इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या
से धीरे-धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। अठारह
पुराणों में अलग-अलग देवी-देवताओं को केन्द्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और
अधर्म, कर्म, और अकर्म की गाथाएँ कही गई हैं।
आज के निरन्तर द्वन्द्व के युग में पुराणों का पठन मनुष्य़ को उस द्वन्द्व से मुक्ति दिलाने में एक निश्चित दिशा दे सकता है और मानवता के मूल्यों की स्थापना में एक सफल प्रयास सिद्ध हो सकता है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पाठकों की रुचि के अनुसार सरल, सहज और भाषा में पुराण साहित्य की श्रृंखला में यह पुस्तक प्रस्तुत है।
पुराण साहित्य भारतीय साहित्य और जीवन की अक्षुण्ण निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती हैं। अठारह पुराणों में अलग-अलग देवी-देवाताओं को केन्द्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कहीं गई हैं। इस में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों की स्थापना आज के मनुष्य को एक निश्चित दिशा दे सकता है।
निरन्तर द्वन्द्व और निरन्तर द्वन्द्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति का मूल आधार है। पुराण हमें आधार देते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पाठकों की रुचि के अनुसार सरल, सहज भाषा में प्रस्तुत है पुराण-साहित्य की श्रृंखला में ‘नारद पुराण’।
आज के निरन्तर द्वन्द्व के युग में पुराणों का पठन मनुष्य़ को उस द्वन्द्व से मुक्ति दिलाने में एक निश्चित दिशा दे सकता है और मानवता के मूल्यों की स्थापना में एक सफल प्रयास सिद्ध हो सकता है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पाठकों की रुचि के अनुसार सरल, सहज और भाषा में पुराण साहित्य की श्रृंखला में यह पुस्तक प्रस्तुत है।
पुराण साहित्य भारतीय साहित्य और जीवन की अक्षुण्ण निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती हैं। अठारह पुराणों में अलग-अलग देवी-देवाताओं को केन्द्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कहीं गई हैं। इस में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों की स्थापना आज के मनुष्य को एक निश्चित दिशा दे सकता है।
निरन्तर द्वन्द्व और निरन्तर द्वन्द्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति का मूल आधार है। पुराण हमें आधार देते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पाठकों की रुचि के अनुसार सरल, सहज भाषा में प्रस्तुत है पुराण-साहित्य की श्रृंखला में ‘नारद पुराण’।
प्रस्तावना
भारतीय जीवन-धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण
भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराण-साहित्य
भारतीय जीवन और साहित्य की अक्षुणय निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष
और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती हैं। भारतीय चिंतन-परंपरा में कर्मकांड
युग, उपनिषद् युग अर्थात् ज्ञान युग और पुराण युग अर्थात् भक्ति युग का
निरंतर विकास होता हुआ दिखाई देता है। कर्मकांड से ज्ञान की ओर आते हुए
भारतीय मानस चिंतन के ऊर्ध्व शिखर पर पहुंचा और ज्ञानात्मक चिंतन के बाद
भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई।
विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे-धीरे भारतीय मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। पुराण साहित्य सामान्यतया सगुण भक्ति का प्रतिपादन करता है। यहीं आकर हमें यह भी मालूम होता है कि सृष्टि के रहस्यों के विषय में भारतीय मनीषियों ने कितना चिंतन और मनन किया है। पुराण साहित्य को केवल कहकर छोड़ देना उस पूरी चिंतन-धारा से अपने को अपरिचित रखना होगा जिसे जाने बिना हम वास्तविक रूप में अपनी परंपरा को नहीं जान सकते।
परंपरा का ज्ञान किसी भी स्तर पर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि परंपरा से अपने को संबद्ध करना और तब आधुनिक होकर उससे मुक्त होना बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। हमारे पुराण-साहित्य में सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसका विकास, मानव उत्पत्ति और फिर उसके विविध विकासात्मक सोपान इस तरह से दिए गए हैं कि यदि उनसे चमत्कार और अतिरिक्त विश्वास के अंश ध्यान में न रखे जाएं तो अनेक बातें बहुत कुछ विज्ञान सम्मत भी हो सकती हैं। क्योंकि जहां तक सृष्टि के रहस्य का प्रश्न है विकासवाद के सिद्धांत के बावजूद और वैज्ञानिक जानकारी के होने पर भी वह अभी तक मनुष्य की बुद्धि के लिए एक चुनौती है और इसलिए जिन बातों का वर्णन सृष्टि के संदर्भ में पुराण-साहित्य में हुआ है उसे एकाएक पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।
महर्षि वेदव्यास को इन 18 पुराणों की रचना का श्रेय है। महाभारत के रचयिता भी वेदव्यास ही हैं। वेदव्यास एक व्यक्ति रहे होंगे या एक पीठ, यह प्रश्न दूसरा है और यह बात भी अलग है कि सारे पुराण कथा-कथन शैली में विकासशील रचनाएं हैं। इसलिए उनके मूल रूप में परिवर्तन होता गया, लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये सारे पुराण तर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना उसमें व्यक्त जीवन-मूल्यों का स्वरूप। यह बात दूसरी है कि जिन जीवन-मूल्यों की स्थापना उस काल में पुराण-साहित्य में की गई, वे हमारे आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक रह गए हैं ? लेकिन साथ में यह भी कहना होगा कि धर्म और धर्म का आस्थामूलक व्यवहार किसी तर्क और मूल्यवत्ता की प्रासंगिकता की अपेक्षा नहीं करता। उससे एक ऐसा आत्मविश्वास और आत्मलोक जन्म लेता है जिससे मानव का आंतरिक उत्कर्ष होता है और हम कितनी भी भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति कर लें अंततः आस्था की तुलना में यह उन्नति अधिक देर नहीं ठहरती। इसलिए इन पुराणों का महत्त्व तर्क पर अधिक आधारित न होकर भावना और विश्वास पर आधारित है और इन्हीं अर्थों में इसका महत्व है।
जैसा कि हमने कहा कि पुराण-साहित्य में अवतारवाद की प्रतिष्ठा है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना का प्रतिपादन इन ग्रन्थों का मूल विषय है। 18 पुराणों में अलग-अलग देवी देवताओं को केन्द्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तथा कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। उन सबसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आखिर मनुष्य और इस सृष्टि का आधा-सौंदर्य तथा इसकी मानवीय अर्थवत्ता में कहीं-न-कहीं सद्गुणों की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। आधुनिक जीवन में भी संघर्ष की अनेक भावभूमियों पर आने के बाद भी विशिष्ट मानव मूल्य अपनी अर्थवत्ता नहीं खो सकते। त्याग, प्रेम, भक्ति सेवा सहनशीलता आदि ऐसे मानव गुण हैं जिनके अभाव में किसी भी बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए भिन्न-भिन्न पुराणों में देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को लेकर मूल्य के स्तर पर एक विराट आयोजन मिलता है। एक बात और आश्चर्यजनक रूप से पुराणों में मिलती है कि सत्कर्म की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में अपकर्म और दुष्कर्म का व्यापक चित्रण करने में पुराणकार कभी पीछे नहीं हटा और उसने देवताओं की कुप्रवृत्तियों को भी व्यापक रूप में चित्रित किया है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है।
कलियुग का जैसा वर्णन पुराणों में मिलता है, आज हम लगभग वैसा ही समय देख रहे हैं। अतः यह तो निश्चिय है कि पुराणकार ने समय के विकास में वृत्तियों को और वृत्तियों के विकास को बहुत ठीक तरह से पहचाना। इस रूप में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों का स्थापन आज के मनुष्य को एक दिशा तो दे सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में अंधविश्वास का विरोध करना तो तर्कपूर्ण है, लेकिन विश्वास का विरोध करना आत्महत्या के समान है।
प्रत्येक पुराण में हजारों श्लोक हैं और उनमें कथा कहने की प्रवृत्ति तथा भक्ति के गुणों की विशेष परक अभिव्यक्ति बार-बार हुई है, लेकिन चेतन और अचेतन के तमाम रहस्यात्मक स्वरूपों का चित्रण, पुनरुक्ति भाव से होने के बाद भी बहुत प्रभावशाली हुआ है और हिन्दी में अनेक पुराण यथावत् लिखे गये फिर यह प्रश्न उठ सकता कि हमने इस प्रकार पुराणों का लेखन और प्रकाशन क्यों प्रारंभ किया। उत्तर स्पष्ट है कि जिन पाठकों तक अपने प्रकाशन की सीमा में अन्य पुराण नहीं पहुंचे होंगे हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस पठनीय साहित्य को उनके सामने प्रस्तुत कर जीवन और जगत् की स्वतंत्र धारणा स्थापित करने का प्रयास कर सकेंगे।
हमने मूल पुराणों में कही हुई बातें और शैली यथावत् स्वीकार की है और सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया है। किंतु जो तत्त्वदर्शी शब्द हैं उनका वैसा ही प्रयोग करने का निश्चय इसलिए किया गया कि उनका ज्ञान हमारे पाठकों को उसी रूप में हो।
हम आज के जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति के बीच से गुजर रहें हैँ। हमारे बहुत सारे मूल्य खंडित हो गए हैं। आधुनिक ज्ञान के नाम पर विदेशी चिंतन का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक हावी हो रहा है इसलिए एक संघर्ष हमें अपनी मानसिकता से ही करना होगा कि अपनी परंपरा जो ग्रहणीय है, मूल्यपरक है उस पर फिर से लौटना होगा। साथ में तार्किक विदेशी ज्ञान भंडार से भी अपरिचित रहना होगा-क्योंकि विकल्प में जो कुछ भी हमें दिया है वह आरोहण और नकल के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है और उस विचित्रता में वि्श्वास और विश्वास का द्वंद्व भी निरंतर होता रहता है। इस द्वंद्व से परे होना ही मनुष्य जीवन का ध्येय हो सकता है। निरंतर द्वंद्व और निरंतर द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति के विकास का यही मूल आधार है। हमारे पुराण हमें आधार देते हैं और यही ध्यान में रखकर हमने सरल सहज भाषा में अपने पाठकों के सामने पुराण-साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें हम केवल प्रस्तोता हैं, लेखक नहीं। जो कुछ हमारे साहित्य में है उसे उसी रूप में चित्रित करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है।
‘डायमंड पॉकेट बुक्स’ के श्री नरेन्द्र कुमार जी के प्रति हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय धार्मिक जनता को अपने साहित्य से परिचित कराने का महत् अनुष्ठान किया है। देवता एक भाव संज्ञा भी है और आस्था का आधार भी। इसलिए वह हमारे लिए अनिवार्य है और यह पुराण उन्हीं के लिए हैं जिनके लिए यह अनिवार्य हैं।
विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे-धीरे भारतीय मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। पुराण साहित्य सामान्यतया सगुण भक्ति का प्रतिपादन करता है। यहीं आकर हमें यह भी मालूम होता है कि सृष्टि के रहस्यों के विषय में भारतीय मनीषियों ने कितना चिंतन और मनन किया है। पुराण साहित्य को केवल कहकर छोड़ देना उस पूरी चिंतन-धारा से अपने को अपरिचित रखना होगा जिसे जाने बिना हम वास्तविक रूप में अपनी परंपरा को नहीं जान सकते।
परंपरा का ज्ञान किसी भी स्तर पर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि परंपरा से अपने को संबद्ध करना और तब आधुनिक होकर उससे मुक्त होना बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। हमारे पुराण-साहित्य में सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसका विकास, मानव उत्पत्ति और फिर उसके विविध विकासात्मक सोपान इस तरह से दिए गए हैं कि यदि उनसे चमत्कार और अतिरिक्त विश्वास के अंश ध्यान में न रखे जाएं तो अनेक बातें बहुत कुछ विज्ञान सम्मत भी हो सकती हैं। क्योंकि जहां तक सृष्टि के रहस्य का प्रश्न है विकासवाद के सिद्धांत के बावजूद और वैज्ञानिक जानकारी के होने पर भी वह अभी तक मनुष्य की बुद्धि के लिए एक चुनौती है और इसलिए जिन बातों का वर्णन सृष्टि के संदर्भ में पुराण-साहित्य में हुआ है उसे एकाएक पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।
महर्षि वेदव्यास को इन 18 पुराणों की रचना का श्रेय है। महाभारत के रचयिता भी वेदव्यास ही हैं। वेदव्यास एक व्यक्ति रहे होंगे या एक पीठ, यह प्रश्न दूसरा है और यह बात भी अलग है कि सारे पुराण कथा-कथन शैली में विकासशील रचनाएं हैं। इसलिए उनके मूल रूप में परिवर्तन होता गया, लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये सारे पुराण तर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना उसमें व्यक्त जीवन-मूल्यों का स्वरूप। यह बात दूसरी है कि जिन जीवन-मूल्यों की स्थापना उस काल में पुराण-साहित्य में की गई, वे हमारे आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक रह गए हैं ? लेकिन साथ में यह भी कहना होगा कि धर्म और धर्म का आस्थामूलक व्यवहार किसी तर्क और मूल्यवत्ता की प्रासंगिकता की अपेक्षा नहीं करता। उससे एक ऐसा आत्मविश्वास और आत्मलोक जन्म लेता है जिससे मानव का आंतरिक उत्कर्ष होता है और हम कितनी भी भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति कर लें अंततः आस्था की तुलना में यह उन्नति अधिक देर नहीं ठहरती। इसलिए इन पुराणों का महत्त्व तर्क पर अधिक आधारित न होकर भावना और विश्वास पर आधारित है और इन्हीं अर्थों में इसका महत्व है।
जैसा कि हमने कहा कि पुराण-साहित्य में अवतारवाद की प्रतिष्ठा है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना का प्रतिपादन इन ग्रन्थों का मूल विषय है। 18 पुराणों में अलग-अलग देवी देवताओं को केन्द्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तथा कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। उन सबसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आखिर मनुष्य और इस सृष्टि का आधा-सौंदर्य तथा इसकी मानवीय अर्थवत्ता में कहीं-न-कहीं सद्गुणों की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। आधुनिक जीवन में भी संघर्ष की अनेक भावभूमियों पर आने के बाद भी विशिष्ट मानव मूल्य अपनी अर्थवत्ता नहीं खो सकते। त्याग, प्रेम, भक्ति सेवा सहनशीलता आदि ऐसे मानव गुण हैं जिनके अभाव में किसी भी बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए भिन्न-भिन्न पुराणों में देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को लेकर मूल्य के स्तर पर एक विराट आयोजन मिलता है। एक बात और आश्चर्यजनक रूप से पुराणों में मिलती है कि सत्कर्म की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में अपकर्म और दुष्कर्म का व्यापक चित्रण करने में पुराणकार कभी पीछे नहीं हटा और उसने देवताओं की कुप्रवृत्तियों को भी व्यापक रूप में चित्रित किया है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है।
कलियुग का जैसा वर्णन पुराणों में मिलता है, आज हम लगभग वैसा ही समय देख रहे हैं। अतः यह तो निश्चिय है कि पुराणकार ने समय के विकास में वृत्तियों को और वृत्तियों के विकास को बहुत ठीक तरह से पहचाना। इस रूप में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों का स्थापन आज के मनुष्य को एक दिशा तो दे सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में अंधविश्वास का विरोध करना तो तर्कपूर्ण है, लेकिन विश्वास का विरोध करना आत्महत्या के समान है।
प्रत्येक पुराण में हजारों श्लोक हैं और उनमें कथा कहने की प्रवृत्ति तथा भक्ति के गुणों की विशेष परक अभिव्यक्ति बार-बार हुई है, लेकिन चेतन और अचेतन के तमाम रहस्यात्मक स्वरूपों का चित्रण, पुनरुक्ति भाव से होने के बाद भी बहुत प्रभावशाली हुआ है और हिन्दी में अनेक पुराण यथावत् लिखे गये फिर यह प्रश्न उठ सकता कि हमने इस प्रकार पुराणों का लेखन और प्रकाशन क्यों प्रारंभ किया। उत्तर स्पष्ट है कि जिन पाठकों तक अपने प्रकाशन की सीमा में अन्य पुराण नहीं पहुंचे होंगे हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस पठनीय साहित्य को उनके सामने प्रस्तुत कर जीवन और जगत् की स्वतंत्र धारणा स्थापित करने का प्रयास कर सकेंगे।
हमने मूल पुराणों में कही हुई बातें और शैली यथावत् स्वीकार की है और सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया है। किंतु जो तत्त्वदर्शी शब्द हैं उनका वैसा ही प्रयोग करने का निश्चय इसलिए किया गया कि उनका ज्ञान हमारे पाठकों को उसी रूप में हो।
हम आज के जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति के बीच से गुजर रहें हैँ। हमारे बहुत सारे मूल्य खंडित हो गए हैं। आधुनिक ज्ञान के नाम पर विदेशी चिंतन का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक हावी हो रहा है इसलिए एक संघर्ष हमें अपनी मानसिकता से ही करना होगा कि अपनी परंपरा जो ग्रहणीय है, मूल्यपरक है उस पर फिर से लौटना होगा। साथ में तार्किक विदेशी ज्ञान भंडार से भी अपरिचित रहना होगा-क्योंकि विकल्प में जो कुछ भी हमें दिया है वह आरोहण और नकल के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है और उस विचित्रता में वि्श्वास और विश्वास का द्वंद्व भी निरंतर होता रहता है। इस द्वंद्व से परे होना ही मनुष्य जीवन का ध्येय हो सकता है। निरंतर द्वंद्व और निरंतर द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति के विकास का यही मूल आधार है। हमारे पुराण हमें आधार देते हैं और यही ध्यान में रखकर हमने सरल सहज भाषा में अपने पाठकों के सामने पुराण-साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें हम केवल प्रस्तोता हैं, लेखक नहीं। जो कुछ हमारे साहित्य में है उसे उसी रूप में चित्रित करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है।
‘डायमंड पॉकेट बुक्स’ के श्री नरेन्द्र कुमार जी के प्रति हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय धार्मिक जनता को अपने साहित्य से परिचित कराने का महत् अनुष्ठान किया है। देवता एक भाव संज्ञा भी है और आस्था का आधार भी। इसलिए वह हमारे लिए अनिवार्य है और यह पुराण उन्हीं के लिए हैं जिनके लिए यह अनिवार्य हैं।
-डॉ. विनय
नारद पुराण का महत्त्व
नारद पुराण परम पुनीत सर्व कष्ट निवारक, सर्व सुख प्रदाता पुराण है। इस
परम पुनीत पुराण में प्रवृत्ति और निवृत्ति का सार गर्भित एवं विस्तृत
विवेचन किया गया है वैसा अन्य जगह मिलना दुर्लभ है।
यह पुराण नैमिषारण्य में एक बहुत बड़े सम्मेलन से शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में मुख्यतः चार विषयों पर गम्भीर विचार हुआ जैसे पृथ्वी पर कौन-कौन-से क्षेत्र पवित्र हैं..., विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति पाने का सरल उपाय..., आदि। महर्षि शोनक ने सुझाया महाराज सूतजी सर्वश्रेष्ठ पौराणिक प्रवक्ता हैं। इसलिए समस्या का समाधान सूतजी ही कर सकते हैं। सूतजी ने बड़ी शान्ति से जिज्ञासाओं की प्रश्नावली सुनकर इन सभी शंकाओं का निराकरण करने के लिए नारद पुराण को सुनाया। यह पुराण सभी पापों को नाश करने वाला है, दुःस्वप्न की चिन्ता का निवारण करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का हेतुरूप है।
यह पुराण परम गोपनीय है साथ ही यह केवल श्रद्धालु एवं निष्ठावान भक्तों के लिए ही प्रयोग योग्य है। इसका वाचन किसी पवित्र स्थान पर होना चाहिए। यह मूल रूप से वैष्णव प्रकृति व प्रवृत्ति का पुराण है। इसे दो खण्डों में विभाजित किया है। प्रथम खंड के शुरुआत में इसमें ब्रह्माजी के चार मानव पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, तथा सनत्कुमार की कथा है। जिसमें उन्होंने नारद जी से कुछ शंकाओं का निवारण करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मार्कण्डेय की कथा सुनाई। तीर्थ गंगा के महत्त्व व पूजन को बताया गया है। उसके आगे सूर्यवंशी राजा वृक के बाहु की कथा है। जिसमें आगे जाकर कपिल मुनि द्वारा सगर पुत्रों को भस्म करने की तथा अंशुमान को गंगा को नीचे उतारकर उनके उद्धार तक की कथा है। आगे गुरु का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मराक्षस ने बारह प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया है।
आगे सनक मुनि द्वारा भगवान् विष्णु के वामन रूप में देवताओं के संकट दूर करने और बलि के अहंकार को नष्ट करने की कथा कही गई है।
इसमें अन्नदान, विद्यादान से प्राप्त होने वाले लोगों के बारे में बताया है। बुद्धिमान् व्यक्ति के द्वारा पांच प्रकार के श्राद्ध को बताया है, परस्त्रीगामियों, विश्वासघात करने वालों, मंदिर में अथवा सरोवर में मल त्याग करने, वेद और चंदनादि आदि गलत कार्य करने वालों को किस तरह का नरक भुगतना पड़ता है का सविस्तार वर्णन आगे सनक मुनि ने नारदजी की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हुए उनसे सत्कर्मों का उल्लेख किया है।
द्वितीय खंड में समस्त तपों, व्रतों धर्मानुष्ठानों एवं दान आदि के निष्पादन की विधियां हैं, नियत काल है एवं तिथियां हैं। इसके अन्तर्गत गौ वध होने पर प्रायश्चित, चोरी में प्रायश्चित, आनजाने में मां बहन से यौन संसर्ग करने पर प्रायश्चित के तरीके बताए गए हैं। आगे विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही इसमें बताया है ब्रह्माजी का एक दिन होता है एक में चौदह मनु, चौदह इंद्र और चौदह ही प्रकार के भिन्न-भिन्न देवता होते हैं। इसकी तालिका दी गई है। सत्ययुग से लेकर कलियुग के बारे में बताया गया है। अंत में वेद के अंगों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्दों का वर्णन है। अतः इसे पुराण का श्रवण और श्री नारायण में श्रद्धापूर्वक अनुरक्ति से मनुष्य अपने जीवन का सफल काम करता हुआ मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। श्री नारद पुराण श्रेष्ठ है इसका पठन एवं श्रवण उपकारी है। अंततः यह कहेंगे इस पुराण में गोपनीय अनुष्ठान, धर्मनिरूपण तथा भक्ति महत्त्वपरक विलक्षण कथाएं आदि का अलौकिक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान प्राप्त होता है।
यह पुराण नैमिषारण्य में एक बहुत बड़े सम्मेलन से शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में मुख्यतः चार विषयों पर गम्भीर विचार हुआ जैसे पृथ्वी पर कौन-कौन-से क्षेत्र पवित्र हैं..., विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति पाने का सरल उपाय..., आदि। महर्षि शोनक ने सुझाया महाराज सूतजी सर्वश्रेष्ठ पौराणिक प्रवक्ता हैं। इसलिए समस्या का समाधान सूतजी ही कर सकते हैं। सूतजी ने बड़ी शान्ति से जिज्ञासाओं की प्रश्नावली सुनकर इन सभी शंकाओं का निराकरण करने के लिए नारद पुराण को सुनाया। यह पुराण सभी पापों को नाश करने वाला है, दुःस्वप्न की चिन्ता का निवारण करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का हेतुरूप है।
यह पुराण परम गोपनीय है साथ ही यह केवल श्रद्धालु एवं निष्ठावान भक्तों के लिए ही प्रयोग योग्य है। इसका वाचन किसी पवित्र स्थान पर होना चाहिए। यह मूल रूप से वैष्णव प्रकृति व प्रवृत्ति का पुराण है। इसे दो खण्डों में विभाजित किया है। प्रथम खंड के शुरुआत में इसमें ब्रह्माजी के चार मानव पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, तथा सनत्कुमार की कथा है। जिसमें उन्होंने नारद जी से कुछ शंकाओं का निवारण करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मार्कण्डेय की कथा सुनाई। तीर्थ गंगा के महत्त्व व पूजन को बताया गया है। उसके आगे सूर्यवंशी राजा वृक के बाहु की कथा है। जिसमें आगे जाकर कपिल मुनि द्वारा सगर पुत्रों को भस्म करने की तथा अंशुमान को गंगा को नीचे उतारकर उनके उद्धार तक की कथा है। आगे गुरु का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मराक्षस ने बारह प्रकार के गुरुओं का उल्लेख किया है।
आगे सनक मुनि द्वारा भगवान् विष्णु के वामन रूप में देवताओं के संकट दूर करने और बलि के अहंकार को नष्ट करने की कथा कही गई है।
इसमें अन्नदान, विद्यादान से प्राप्त होने वाले लोगों के बारे में बताया है। बुद्धिमान् व्यक्ति के द्वारा पांच प्रकार के श्राद्ध को बताया है, परस्त्रीगामियों, विश्वासघात करने वालों, मंदिर में अथवा सरोवर में मल त्याग करने, वेद और चंदनादि आदि गलत कार्य करने वालों को किस तरह का नरक भुगतना पड़ता है का सविस्तार वर्णन आगे सनक मुनि ने नारदजी की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हुए उनसे सत्कर्मों का उल्लेख किया है।
द्वितीय खंड में समस्त तपों, व्रतों धर्मानुष्ठानों एवं दान आदि के निष्पादन की विधियां हैं, नियत काल है एवं तिथियां हैं। इसके अन्तर्गत गौ वध होने पर प्रायश्चित, चोरी में प्रायश्चित, आनजाने में मां बहन से यौन संसर्ग करने पर प्रायश्चित के तरीके बताए गए हैं। आगे विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही इसमें बताया है ब्रह्माजी का एक दिन होता है एक में चौदह मनु, चौदह इंद्र और चौदह ही प्रकार के भिन्न-भिन्न देवता होते हैं। इसकी तालिका दी गई है। सत्ययुग से लेकर कलियुग के बारे में बताया गया है। अंत में वेद के अंगों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्दों का वर्णन है। अतः इसे पुराण का श्रवण और श्री नारायण में श्रद्धापूर्वक अनुरक्ति से मनुष्य अपने जीवन का सफल काम करता हुआ मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। श्री नारद पुराण श्रेष्ठ है इसका पठन एवं श्रवण उपकारी है। अंततः यह कहेंगे इस पुराण में गोपनीय अनुष्ठान, धर्मनिरूपण तथा भक्ति महत्त्वपरक विलक्षण कथाएं आदि का अलौकिक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान प्राप्त होता है।
नारद पुराण
एक बार नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में
बड़े-बड़े तपस्वी, तत्त्वज्ञानी और स्वाध्याय प्रेमी ऋषि मुनि पधारे। इस
सम्मेलन में मुख्यतः इन चार विषयों पर गम्भीर विचार हुआ।
1. इस पृथ्वी पर कौन-कौन से क्षेत्र पवित्र हैं और तीर्थ स्थान हैं जहां वास करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है ?
2. इस संसार में आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापों से दुःखी मनुष्यों की मुक्ति का सरल उपाय क्या हो सकता है ?
3. विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति पाने का सरल उपाय क्या है?
4. दैनिक धर्म कर्म करते हुए मनुष्य अपने दायित्व का पालन करते हुए किस तरह अपना अभीष्ट पूर्ण कर सकता है।
सभी महर्षियों एवं मुनियों ने अपने-अपने विचार रखे। सभी के भिन्न मत देखकर महर्षि शौनक ने उसमें सामंजस्य की भावना से संबोधित करते हुए यह सुझाया कि महाराज सूतजी सर्वश्रेष्ठ पौराणिक प्रवक्ता हैं। ये श्री लोमहर्षण के सुपुत्र और महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं। अतः यदि हम सब वास्तव में अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सिद्धारम में विष्णुभक्ति में लीन सूतजी के समक्ष चलना होगा।
सम्मेलन में उपस्थित सभी ऋषियों ने शौनक मुनि के प्रस्ताव को स्वीकार कर सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान किया। सूतजी ने सभी ऋषियों का यथोचित स्वागत सत्कार किया और विश्राम के पश्चात् उनसे आने का प्रयोजन पूछा। जिज्ञासु मुनियों ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हे प्रभु ! आप सर्वज्ञानी हैं कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करें-
1. त्रिलोकीनाथ और संसार के रचना करने वाले,पालन करने वाले और प्रलयंकारी भगवान् विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को क्या उपाय करने चाहिए ?
2. मनुष्य को सांसारिक आवागमन से मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए ?
3. ईश्वर भक्ति से क्या प्रभाव पड़ता है तथा ईश्वरभक्तों का स्वरूप कैसा होता है ?
4. अतिथियों का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए ?
5. आश्रम तथा वर्ण-व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या है ?
तत्त्वज्ञानी सूतजी ने बड़ी शांति से जिज्ञासुओं की प्रश्नावली सुनकर इन सभी शकाओं का निराकरण करने के लिए नारद पुराण सुनाने का उपक्रम किया। सूतजी ने बताया कि वेदाशास्त्रसम्मत यह पुराण सभी पापों का नाश करने वाला, अनिष्ट दूर करने वाला, दुःस्वप्न और चिन्ता का निराकरण करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह धर्म, अर्थ काम मोक्ष का हेतुरूप है। यह पुराण आख्यान इतना अधिक प्रभावकारी है कि शुद्ध मन से इसका श्रणव करने से ब्रह्महत्या, मदिरापान गुरुपत्नी-रमण जैसे महापातकों और मांस भक्षण वैश्यागमन जैसे उपपातकों से भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाता है।
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मूलनक्षत्र में मथुरा में स्नान करके विधिवत् व्रत-उपवास करके भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करते हुए श्री नारद पुराण का श्रवण करें तो भक्ति जन्म-जन्मान्तरों के पाप से मुक्त हो जाता है। माया के जाल से मुक्त होकर निरंजन हो जाता है। भगवान् विष्णु के चरणों में वृत्ति रखने वाला संसार के प्रति अनासक्त होकर फलस्वरूप जीव मुक्ति को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ वासी हो जाता है।
सूतजी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पुराण परम गोपनीय है। यह केवल श्रद्धालु एवं निष्ठानवान भक्तों के लिए ही प्रयोग योग्य है। इसीलिए असत् कर्मों में लिप्त, ब्राह्मणद्रोही, ढोंगी दंभी छपी-कपटी को भूलकर भी इसका श्रवण नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि भगवान् भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस नारद पुराण में श्री विष्णु भगवान् की लीलाओं और महिमा का बड़ा ही मनोरम वर्णन है जिसके सुनने से भक्त सभी राग-विराग, द्वेषभाव से मुक्त विष्णु के अनुराग में उन्हीं का होकर रह जाता है।
यह नारद पुराण स्वयं पवित्र है इसलिए वाचन किसी पवित्र स्थान पर होना चाहिए। जिसके लिए कोई भी मंदिर कोई तीर्थ अथवा एकांत, शांत-स्थान और वाचक स्वयं शुद्ध पवित्र भाव वाला, जन्म से ब्राह्मण विद्वान् और आचारवान होना चाहिए। श्रोता को एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करना चाहिए। यह आवश्यक है कि श्री नारद पुराण का श्रवण शुद्ध मन से, निःस्वार्थ भाव और बिना किसी प्रदर्शन के करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्वक या दंभ में, शुद्ध भावना के अभाव में केवल, प्रदर्शन के लिए नारद पुराण सुनता है तो ऐसा व्यक्ति अनन्त काल तक घोर नारकीय यातनायें सहता है अर्थात् शुद्ध चित्तवृत्ति से ही उसका पारायण लाभप्रद है। वेद निन्दा करने वालों के समान ही पुराण निन्दा करने वाले भी नास्तिक ही होते हैं। भगवान् वेद व्यास ने यह पुराणआख्यान जीवों के कल्याण के लिए ही रचा है। इसलिए इसका श्रवणआराधन चित्तवृत्तियों को केन्द्रित करके पूर्ण श्रद्धाभक्ति से करना चाहिए। मनुष्य के जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टाय को प्राप्त करने में ही है और इसका सरल उपाय सकल विश्व के स्वामी सर्वव्यापी, अनित्य, अमर और सर्वान्तरयामी श्री विष्णु में अटूट भक्ति है। पुराणों का श्रवण इस भक्ति का सरलतम साधन है। इन कथाओं के श्रवण भक्त का भगवान् में मन लग जाता है तथा जन्म-मरण के झंझटों से वह निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। यह कहते हुए महर्षि सूतजी ने ऋषियों से कहा कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के गूढ़ तत्त्वों को प्रकाशित करने वाला पुराणों में विशिष्ट यह नारद पुराण मैं आपको सुनाता हूं। मुझे विश्वास है-यदि शुद्ध मन से आपने इसका श्रवण किया तो आपकी सभी जिज्ञासाओं और शंकाओं का निराकरण हो जायेगा।
1. इस पृथ्वी पर कौन-कौन से क्षेत्र पवित्र हैं और तीर्थ स्थान हैं जहां वास करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है ?
2. इस संसार में आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापों से दुःखी मनुष्यों की मुक्ति का सरल उपाय क्या हो सकता है ?
3. विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति पाने का सरल उपाय क्या है?
4. दैनिक धर्म कर्म करते हुए मनुष्य अपने दायित्व का पालन करते हुए किस तरह अपना अभीष्ट पूर्ण कर सकता है।
सभी महर्षियों एवं मुनियों ने अपने-अपने विचार रखे। सभी के भिन्न मत देखकर महर्षि शौनक ने उसमें सामंजस्य की भावना से संबोधित करते हुए यह सुझाया कि महाराज सूतजी सर्वश्रेष्ठ पौराणिक प्रवक्ता हैं। ये श्री लोमहर्षण के सुपुत्र और महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं। अतः यदि हम सब वास्तव में अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सिद्धारम में विष्णुभक्ति में लीन सूतजी के समक्ष चलना होगा।
सम्मेलन में उपस्थित सभी ऋषियों ने शौनक मुनि के प्रस्ताव को स्वीकार कर सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान किया। सूतजी ने सभी ऋषियों का यथोचित स्वागत सत्कार किया और विश्राम के पश्चात् उनसे आने का प्रयोजन पूछा। जिज्ञासु मुनियों ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हे प्रभु ! आप सर्वज्ञानी हैं कृपया हमारी जिज्ञासा शांत करें-
1. त्रिलोकीनाथ और संसार के रचना करने वाले,पालन करने वाले और प्रलयंकारी भगवान् विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को क्या उपाय करने चाहिए ?
2. मनुष्य को सांसारिक आवागमन से मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए ?
3. ईश्वर भक्ति से क्या प्रभाव पड़ता है तथा ईश्वरभक्तों का स्वरूप कैसा होता है ?
4. अतिथियों का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए ?
5. आश्रम तथा वर्ण-व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या है ?
तत्त्वज्ञानी सूतजी ने बड़ी शांति से जिज्ञासुओं की प्रश्नावली सुनकर इन सभी शकाओं का निराकरण करने के लिए नारद पुराण सुनाने का उपक्रम किया। सूतजी ने बताया कि वेदाशास्त्रसम्मत यह पुराण सभी पापों का नाश करने वाला, अनिष्ट दूर करने वाला, दुःस्वप्न और चिन्ता का निराकरण करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह धर्म, अर्थ काम मोक्ष का हेतुरूप है। यह पुराण आख्यान इतना अधिक प्रभावकारी है कि शुद्ध मन से इसका श्रणव करने से ब्रह्महत्या, मदिरापान गुरुपत्नी-रमण जैसे महापातकों और मांस भक्षण वैश्यागमन जैसे उपपातकों से भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाता है।
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मूलनक्षत्र में मथुरा में स्नान करके विधिवत् व्रत-उपवास करके भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करते हुए श्री नारद पुराण का श्रवण करें तो भक्ति जन्म-जन्मान्तरों के पाप से मुक्त हो जाता है। माया के जाल से मुक्त होकर निरंजन हो जाता है। भगवान् विष्णु के चरणों में वृत्ति रखने वाला संसार के प्रति अनासक्त होकर फलस्वरूप जीव मुक्ति को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ वासी हो जाता है।
सूतजी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पुराण परम गोपनीय है। यह केवल श्रद्धालु एवं निष्ठानवान भक्तों के लिए ही प्रयोग योग्य है। इसीलिए असत् कर्मों में लिप्त, ब्राह्मणद्रोही, ढोंगी दंभी छपी-कपटी को भूलकर भी इसका श्रवण नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि भगवान् भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस नारद पुराण में श्री विष्णु भगवान् की लीलाओं और महिमा का बड़ा ही मनोरम वर्णन है जिसके सुनने से भक्त सभी राग-विराग, द्वेषभाव से मुक्त विष्णु के अनुराग में उन्हीं का होकर रह जाता है।
यह नारद पुराण स्वयं पवित्र है इसलिए वाचन किसी पवित्र स्थान पर होना चाहिए। जिसके लिए कोई भी मंदिर कोई तीर्थ अथवा एकांत, शांत-स्थान और वाचक स्वयं शुद्ध पवित्र भाव वाला, जन्म से ब्राह्मण विद्वान् और आचारवान होना चाहिए। श्रोता को एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करना चाहिए। यह आवश्यक है कि श्री नारद पुराण का श्रवण शुद्ध मन से, निःस्वार्थ भाव और बिना किसी प्रदर्शन के करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्वक या दंभ में, शुद्ध भावना के अभाव में केवल, प्रदर्शन के लिए नारद पुराण सुनता है तो ऐसा व्यक्ति अनन्त काल तक घोर नारकीय यातनायें सहता है अर्थात् शुद्ध चित्तवृत्ति से ही उसका पारायण लाभप्रद है। वेद निन्दा करने वालों के समान ही पुराण निन्दा करने वाले भी नास्तिक ही होते हैं। भगवान् वेद व्यास ने यह पुराणआख्यान जीवों के कल्याण के लिए ही रचा है। इसलिए इसका श्रवणआराधन चित्तवृत्तियों को केन्द्रित करके पूर्ण श्रद्धाभक्ति से करना चाहिए। मनुष्य के जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टाय को प्राप्त करने में ही है और इसका सरल उपाय सकल विश्व के स्वामी सर्वव्यापी, अनित्य, अमर और सर्वान्तरयामी श्री विष्णु में अटूट भक्ति है। पुराणों का श्रवण इस भक्ति का सरलतम साधन है। इन कथाओं के श्रवण भक्त का भगवान् में मन लग जाता है तथा जन्म-मरण के झंझटों से वह निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। यह कहते हुए महर्षि सूतजी ने ऋषियों से कहा कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के गूढ़ तत्त्वों को प्रकाशित करने वाला पुराणों में विशिष्ट यह नारद पुराण मैं आपको सुनाता हूं। मुझे विश्वास है-यदि शुद्ध मन से आपने इसका श्रवण किया तो आपकी सभी जिज्ञासाओं और शंकाओं का निराकरण हो जायेगा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book